Disaster Management in Hindi: आपदा प्रबंधन (Disaster Management) एक बहुस्तरीय योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन) और मानवीय आपदाओं के साथ-साथ बीमारी के तेजी से प्रसार को रोकने इत्यादि मुद्दों पर कार्य करती है। प्रकृति में पाए जाने वाले चार प्रमुख तत्व अग्नि, वर्षा, पवन और पृथ्वी जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, वे विनाशकारी भी हो सकते है। इनसे खेलना इतना नुक्सानदयाक हो सकता है जिसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है।
Table of Contents
देश को हर साल कई प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्यक्तियों एवं जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, वहीं करोड़ों-अरबो रूपये की धन-संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही विषम परिस्थितियों के शिकार बने लोगों की सहायता करने, उन्हें उबारने और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है।
इसलिए मैंने सोंचा क्यों न आपदा प्रबंधन पर निबंध लिखा जाये और आपको आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाएं जैसे- आपदा प्रबंधन क्या है, कितने प्रकार के होते है, आपदा प्रबंधन की भूमिका एवं उनके चरण आदि। साथ ही आप यहां आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है, आपदा प्रबंधन Project in Hindi (आपदा प्रबंधन पर प्रोजेक्ट) के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा आप इस लेख में प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, न्यूनीकरण पर निबंध (Aapda Prabandhan Essay in Hindi), आपदा प्रबंधन के कारण, आपदा प्रबंधन के उपाय और आपदा प्रबंधन पर टिप्पणी (Aapda Prabandhan Par Tippani) के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।
इन्हे भी पढ़े: Essay on Pollution in Hindi – जानिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हिंदी में
Disaster Management in Hindi
आपदा प्रबंधन क्या है (What is Disaster Management in Hindi)
“आपदा प्रबंधन (Disaster Management) एक ऐसी कार्य प्रणाली है, जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक-दूसरे के समांतर भी चलती रहती है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जा सकता है कि, आपदा संभावित समुदाय के भीतर, आपदा की रोकथाम, उसके दुष्प्रभाव को कम करने, जवाबी कार्यवाही और सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय होते हैं।”
मानव एवं प्राकृतिक कारणों से होने वाले दुष्प्रभाव यदि चरम सीमा तक पहुंच जाए, तथा यह दुष्प्रभाव मानव एवं प्रकृति के लिए असहनीय हो जाए और इन्हें नष्ट करने लगे, तो वह प्रकोप में बदलने लगती है।

जब यह असहनीय घटनाएं मानव बस्ती तक पहुंचने लगे एवं मानव समुदाय को एक साथ नुकसान पहुंचने लगे, तो वह आपदा का रूप ले लेती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जो पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। इन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ना ही इन्हें रोका जा सकता है।
परंतु इनके प्रभावों को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है। जिससे कि भौतिक एवं मानवीय क्षति कम की जा सके। यह कार्य तभी किया जा सकता है, जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। यदि इस कार्य में आपदा प्रबंधन का सहयोग ना मिले, तो कार्य सुचारु रुप से नहीं चल सकता है।
विश्व के किसी भी देश में प्रायः बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सुनामी की घटनाएं होती रहती है। “आपदा प्रबंधन” इनके प्रभाव को कम करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है, जिसे सफल बनाने के लिए सामूहिक एकता एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है।
Aapda Prabandhan in Hindi (आपदा प्रबंधन हिंदी में)
आपदा प्रबंधन पर निबंध
जैसा कि हम लोग जानते है कि विश्व के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अत्याधिक विकास हुआ है। इससे मानव जीवन को अधिक सुखी एवं समृद्ध बना है। परंतु इसके पश्चात मानव जीवन पर अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हुए। हर पल अब मानव इन आपदाओं से अपने को असुरक्षित महसूस करता है। तो चलिए जानते है आपदा प्रबंधन क्या है।
“आपदा” समाज के सामान्य कार्य प्रणाली में बाधा करती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की भी बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदाएं कठिनाइयां पैदा करती है जिससे कि राष्ट्र का विकास कई वर्ष पीछे खिसक जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आपदाओं के फल स्वरुप जान और संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचता है, वह विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक होता है।
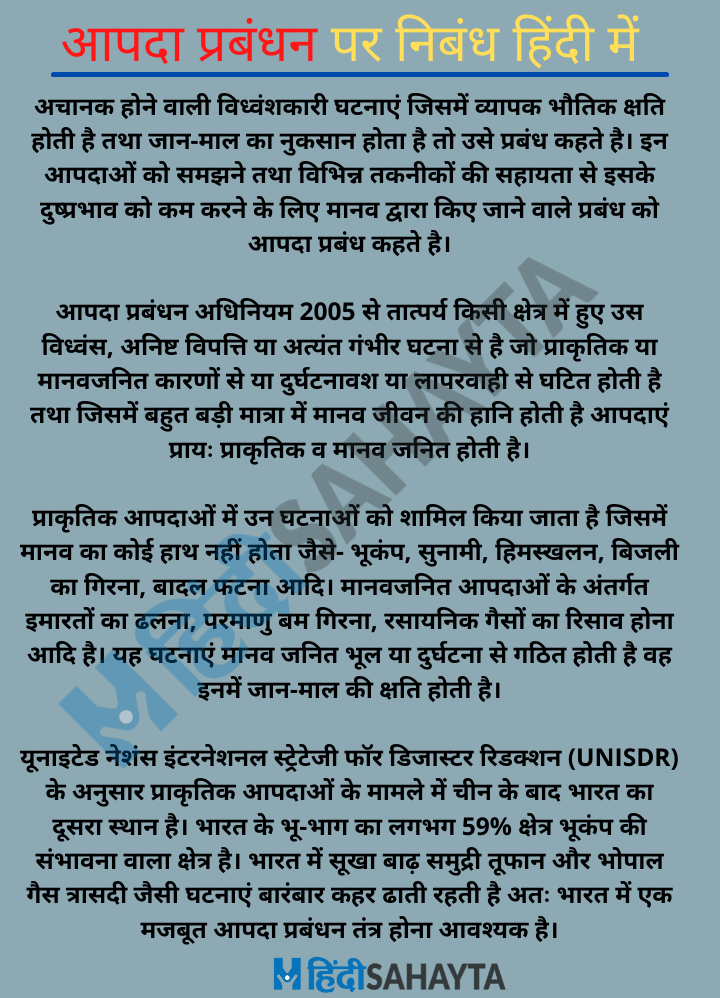
यदि इन आपदाओं के लिए पूर्व तैयारियां नहीं की जाए, तो यह किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनका प्रबंध करना।
चलिए अब आगे जानते है कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट फाइल (Project on Disaster Management) कैसे बनाए। यह जानकारी आपको आपदा प्रबंधन प्रोजेक्ट फाइल इन हिंदी (Disaster Management Project in Hindi) में बनने में भी काम आएगी।
आपदाओं के प्रकार
आईये जानते हैं, कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है?
भारत में कई तरह के संकट देखे गए हैं, जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण है जिन्हे हम 2 वर्गों में समझते है।
- प्राकृतिक आपदाएं: सुखा बाढ़ भूकंप भूस्खलन एवं सुनामी व समस्त घटनाएं हैं, जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं, और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है। इन प्राकृतिक घटनाओं में मानव का किसी भी प्रकार से हाथ नहीं होता। इन प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है।
- मानवनिर्मित आपदाएं: मनुष्य जब अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और वे प्रभाव प्रकृति के लिए विनाशकारी होते हैं। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव कार्यों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रुप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदाई है।
इन संकटों की कतार बहुत लंबी है, और इनमे से कुछ बिंदुओं पर हमने नीचे रौशनी डाली है।
- ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती है – भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़ चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट आदि।
- आपदा जो धीरे-धीरे प्रकट होती है – सूखा, ओले, संक्रामक रोग, आदि।
- महामारी – जल/ खाद आधारित रोग, संक्रामक रोग, आदि।
- औद्योगिक दुर्घटनाएं – आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव इत्यादि।
- युद्ध।
प्राकृतिक आपदाएं
1. सूखा आपदा – सुखा एक प्राकृतिक आपदा है। जल मानव जीवन के लिए मुख्य घटक है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा क्षेत्र जहां पर 25% या उससे कम वर्षा होती है, उसे सूखे क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। निरंतर 2 वर्षों तक होने वाली वार्षिक वर्षा को अत्यधिक श्रेणी में रखा जाता है। कई पशु-पक्षी सूखे के कारण प्यास से जूझकर मर जाते है। आज भी भारत के कई क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी हुई है, कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सूखे का आगमन धीरे-धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है।

सूखा आपदा प्रबंधन एवं उपाय।
- सूखे की स्थिति पर निगाह रखनी चाहिए। निगाह रखने का मतलब है, झीलों, नदियों, तालाबों में पानी की मात्रा पर दृष्टि रखना। सूखा आपदा से बचने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जल संग्रहण को बढ़ावा देना।
- सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है कि खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़े।
- जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरों तथा किसानों के खेतों में वर्षा के पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है।सभी खेतों में बह रहे जल को एक स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए।
2. बाढ़ आपदा – बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा हैं, जिससे एक बड़े भू भाग में पानी भर जाता है, और उस पानी से जन धन की अपार हानि होती है। तालाबों में पानी की वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लाने अथवा तेज हवाओं और चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से, विशाल क्षेत्रों में स्थाई रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। इस संकट से निपटने के लिए और पुनः अपने जीवन को स्थापित करने के लिए मनुष्य को कई वर्ष लग जाते हैं। बाढ़ से प्वनस्पति का भी भारी नुकसान होता है।
बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं उपाय।
- नदियों के ऊपरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाए जाए।
- वह स्थान जहां जल संग्रहण हो रहा हो, वहां आस-पास की जगह पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
- नदियों के किनारे की भूमि पर मानव बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए।
- पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
- सहायक नदियों पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाएं जिससे की मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके।
3. भूकंप आपदा – भूकंप किसी भी समय अचानक, बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा होती है, तथा कंपन होता है। यह कंपन तरंगों के रूप में जैसे-जैसे केंद्र से दूर जाता है, यह तेज होता जाता है। भूकंप का रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उस स्थान मे बड़ी संख्या में जान-माल की हानि होती है। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की सतह बड़ी-बड़ी प्लेटों से बनी है यह प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती है, इनके खिसकने अथवा फैलने से भूकंप आता है।
भूकंप आपदा प्रबंधन एवं उपाय।
- भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों की डिजाइन इंजीनियर के सहयोग से तय होना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों या इमारतों की डिजाइन इंजीनियर के सहयोग से तय होना चाहिए।
- किसी भी इमारत निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण कराना जरूरी होता है। नरम मिट्टी के ऊपर मकान नहीं बनाए जाने चाहिए।
- लोगों के बीच भूकंप को लेकर जागरूकता बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि वह ऐसे स्थान पर भू निर्माण ना करें जहां भूकंप का खतरा अधिक होता है।
4. भूस्खलन आपदा – चट्टानों मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर, जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलान अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन धीरे-धीरे होते हैं, फिर भी आकस्मिक भूस्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। भूस्खलन होने के बारे में कोई पक्की चेतावनी मौजूद नहीं है, अतः इस आपदा घटने का पूर्व अनुमान लगाना कठिन है। भूस्खलन के लिए प्रमुखता भूकंप बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदाई होती है। पहाड़ी क्षेत्र में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने अथवा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र बनाना भी भूस्खलन को जन्म देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टानें एवं मिट्टी खिसकने लगती है। यह अत्यधिक खतरनाक होती है।
भूस्खलन आपदा प्रबंधन एवं उपाय।
- किसी भी बस्तियों के बसने से पहले भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना आवश्यक होता है।
- अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य तथा विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए।
- पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे पहाड़ जहां वनस्पति नहीं है, वह ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को रोपित करके पुनः वनस्पति युक्त बनाया जाना आवश्यक है।
- मजबूत बुनियाद के साथ नक्शा तैयार करके बनाए गए घरों की की भूमि के नीचे बिछाए गए पाइपलाइन केबल्स लचीले होना चाहिए ताकि वह भूस्खलन से उत्पन्न दबाव को सामना आसानी से कर सकें।
5. सुनामी आपदा – भूकंप और ज्वालामुखी से समुद्र के धरातल में तरंग पैदा होती है। यह जल-तरंग बड़े-बड़े समुद्रों में सुनामी लहरों को पैदा करती है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है, और ऊंचाई कम। सुनामी से समुद्री तट वाले क्षेत्र में भीषण हानि होती है। सामान्यता शुरुआत में एक साधारण तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक बड़ी श्रंखला बन जाती है। समुद्री जल कभी भी शांत नहीं रहता, इसमें हलचल होना स्वाभाविक बात है। भूकंप और ज्वालामुखी का समुद्री क्षेत्रों में आना ही सुनामी आपदा का प्रमुख कारण है।

सुनामी आपदा प्रबंधन एवं उपाय।
सुनामी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इससे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। सुनामी को रोका नहीं जा सकता परंतु पहले से चेतावनी मिलने पर तटीय क्षेत्र खाली कर देना ही उपाय है।
मानव निर्मित आपदाएं

1. बम विस्फोट – अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों एवं ऐसे स्थानों पर जहां अधिक मात्रा में मनुष्य उपस्थित हो वहां रखी जाती है।
इससे सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय है।
- यदि कहीं कोई पैकेट नजर आता है और समझा होता है तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अतः उसे छूना नहीं चाहिए।
- संदिग्ध वस्तुओं के पास न तो स्वयं जाना चाहिए ना ही दूसरों को जाने देना चाहिए।
- पुलिस को सूचित करना चाहिए।
2. जैविक एवं रासायनिक आपदा – आज का युग विज्ञान का है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखी व समृद्ध शाली बनाया है।
रासायनिक गैस रिसाव, भोपाल में घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक – रासायनिक आपदा है। इसमें 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से, रात लगभग 12:00 बजे रिसी और हवा के साथ बह गई। इसमें लगभग 3600 लोग मरे और अनेक रोग ग्रस्त हो गए।
टिड्डी दल का आक्रमण कीटों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे प्लेग, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू , डेंगू , कोरोना जैविक आपदाएं है। इनसे बचने के लिए भी उपाय करना आवश्यक है।
औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव निर्मित आपदाएं हैं। इनकी शुरुआत बड़ी तेजी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है।
जैविक दुष्प्रभाव को कम करने के संभावित उपाय।
- खतरनाक रसायनों के उपयोग तथा बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी आम नागरिक तक पहुंचाना चाहिए।
- जहरीले पदार्थों के भंडार की क्षमता सीमित ही रखी जाए।
- उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू होना चाहिए।
- दुर्घटना की स्थिति का मुकाबला करने की समझ विकसित करने हेतु समय-समय पर नकली अभ्यास कराना चाहिए।
इसे भी पढ़ना न भूले: Samay Ka Mahatva – समय के महत्व पर निबंध।
आपदा प्रबंधन पर निबंध हिंदी में
(आपदा प्रबंधन Hindi Essay)
“डिजास्टर या आपदा” का अर्थ होता है, ऐसी घटनाएं जो मानव के जीवन के लिए संकट पैदा करें। प्रबंधन का अर्थ होता है इन घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए की जाने वाले कार्य।
आपदाओं से बड़े पैमान पर हानि होती है, यदि इन आपदाओं के लिए पूर्व प्रबंध नहीं किया जाए, तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इस कारण किसी भी देश के लिए आपदा प्रबंधन बहुतआवश्यक होता है।
“आपदा प्रबंधन” से यह मानकर चला जा सकता है कि आपदा को रोकने, उसके दुष्प्रभाव को कम करने, आपदा के बाद जवाबी कार्यवाही और सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय है।
डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि आपदा क्षेत्र मैं जरूरी सामग्री पहुंचाना एवं पहले से चेतावनी देने के लिए कार्य करना। साथ ही लोगों को आपदा के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है।
आपदा के बाद बाद लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करना एवं लोगों को बचाने के लिए बचाव दलों को भेजना बहुत आवश्यक है। आपदा क्षेत्रों को ढूंढकर वहां के लोगो के लिए अन्य स्थान पर आश्रय की व्यवस्था करना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है।
इसके अंतर्गत किसी भी आपदा के बाद सबसे जरूरी होता है, लोगों को स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, तथा सड़क को और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना। इस प्रबंधन के अंतर्गत आपदा क्षेत्र र्निर्माण किया जाता है।
आपदाओं को कम तो नहीं किया जा सकता, मगर उनसे लोगों को कम क्षति हो, इसके लिए हल खोजना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है।
आपदा प्रबंधन के महत्व पर निबंध
(Aapda Prabandhan Ke Mahatv Par Nibandh)
आपदा प्रबंधन में आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने के लिए कार्य किया जाता है। जैसे कि लोगों को जागरूक करना और शिक्षा पहुंचाना। साथ ही लोगों को आपदा को लेकर चेतावनी जारी करना तथा सतर्क रहने के लिए समझाना।
किसी भी आपदा से पहले और उसके तुरंत बाद आपदा को प्रभाव को कम करने के लिए, एवं संसाधन जुटाने के लिए आपदा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपदा आती है, वह वहां के संसाधनों को भी नष्ट कर देती है।
आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करना तथा प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढ कर बचाव के लिए दल भेजना, आपदा प्रबंधन की मुख्य भूमिका है।
किसी आपदा के खत्म होने के बाद, क्षेत्र के फिर से निर्माण तथा जिनके परिजन बिछड़ गए हो उन्हें दिलासा देने और भावनात्मक रूप से सहायता करने के लिए आपदा प्रबंधन सहायक है।
आपदाओं की रोकथाम उनके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए नई योजनाओं को तैयार करना तथा डॉक्टर्स, इंजीनियर, एवं अन्य आवश्यक अधिकारियों को तैनात करना इसके अंतर्गत आता है।
आपदा से ग्रसित क्षेत्र की भूमि के उपयोग की योजना तैयार करना और साथ ही आपदा घटने से पहले उनके जोखिमों को कम करने के तरीके तलाशने में, आपदा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है।
एक नजर इस लेख पर भी: महिला सशक्तिकरण पर निबंध – Women Empowerment Essay In Hindi
Disaster Management Essay In Hindi
(आपदा प्रबंधन निबंध हिंदी में)
डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। लोगों को बढ़-चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए, यही सब चीजें आपदा प्रबंधन में सहायता करती है।
आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा की रोकथाम, क्षेत्र के पुनर्निर्माण और लोगो के बचाव के लिए कार्य करती है। और साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष सहायता पहुंचाती है।
कोई भी आपदा मानव के नियंत्रण में नहीं है। इससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा दी गई सेवाओं की अपेक्षा लोगों को बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदा प्रबंधन में सरकार की सहायता करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम को 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हुई। आजा प्रबंधन अधिनियम संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे नए कानून बनाए गए।
डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा से पहले, उसके बाद नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है। यह प्रक्रिया लोगों को अपने सामान्य जीवन स्तर पर लौट आने के लिए पर्याप्त उपाय हैं।
आपदा किसी भी समय किसी भी पल बिना चेतावनी दिए आ सकती है, जिससे कि जन-धन की बहुत हानि होती है। आपदाएं समस्या पैदा करती है, जिससे कि राष्ट्र का विकास बहुत सालों पीछे चला जाता है। इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए, आपदा प्रबंधन की भूमिका सबसे ऊपर है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन हिंदी (The Disaster Management Act, 2005)
डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 28 नवंबर 2005 को राज्य सभा द्वारा, एवं 23 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हुई। आपदा प्रबंधन अधिनियम के 11 अध्याय हैं। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय कानून है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा किसी आपदा की स्तिथि में उससे निपटने के लिए किया जाता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न धाराएं लागू की गई हैं:
धारा 51: बाधा डालने के लिए सजा।
इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है या उसके कर्तव्य पालन में बाधा बनता है, तो उसके खिलाफ धारा 51 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कार्यवाही के अंतर्गत दंड के रूप में उस व्यक्ति को 1 साल की सजा या जुर्माना भी हो सकता है।
धारा 52: झूठे दावे करने पर सजा।
यदि कोई व्यक्ति समर्थ है, इसके बावजूद वह राहत, सहायता, मरम्मत या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की ओर से आपदा के परिणामस्वरूप होता है। तो दंड के रूप में उसे 2 साल की सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है।
धारा 53: पैसा,राहत सामग्री का गबन।
आपदा के समय सरकार द्वारा चलाई गई किसी योजना के बीच, यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी या सामान्य व्यक्ति पैसों का गबन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
धारा 54: गलत सूचना के लिए सजा।
आपदा के समय यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना का प्रसारण करता है, जिससे लोगों के बीच में भय का माहौल बने एवं अव्यवस्था हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 54 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत दंड के रूप में उस व्यक्ति को 1 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
धारा 55 : सरकारी विभाग द्वारा अपराध।
यदि कोई सरकारी विभाग द्वारा, कोई अपराध सामने आता है, तो उस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धारा 55 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
धारा 56 : ड्यूटी में अधिकारी की विफलता।
यदि कोई शासकीय अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, या सेवा देने से बचता है, तो उसके खिलाफ धारा 56 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
धारा 57: सेवा ना देने का जुर्म।
यदि सरकार को आपदा के समय किसी व्यक्ति के संसाधन की आवश्यकता हो और यदि वह व्यक्ति सेवा देने से इनकार करता है तो उस व्यक्ति को धारा 57 के तहत एक साल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है।
धारा 58: कंपनी द्वारा कानून के उल्लंघन के लिए सजा।
यदि कोई कंपनी सरकार द्वारा पारित आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन करती है, एवं उलंघन के समय उपस्थित उस कंपनी के सभी कर्मचारियों पर धारा 58 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
धारा 59: अभियोजना के लिए पूर्व मंजूरी।
सेक्शन या धारा 55 और 56 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहता है, तो उसे धारा 59 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
धारा 60: अपराधों का संज्ञान।
इसके अंतर्गत कोई कोर्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे का संज्ञान तभी लेगा जब वह मुकदमा सरकार या प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया गया हो।
जैसा कि हम सभी जानते है कि, आपदा एक अपेक्षित घटना है। यह ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं।
लंबे समय तक आपदाओं को प्राकृतिक वनों का परिणाम माना जाता है, और मानव को इसका असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं का एकमात्र कारण नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव कार्यों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रुप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदाई है जैसे – भोपाल गैस त्रासदी, युद्ध, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जहरीली गैस वायुमंडल में छोड़ना।
ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी, संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण कुछ मानवीय गतिविधियां सीधे रुप से आपदाओं को बढ़ावा देती है, जैसे वनों के विनाश से भूस्खलन और बाढ़। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रयत्न भी किए गए परंतु सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी परंतु इस मानव निर्मित आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है।
इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके प्रभाव को कम करना और इनका प्रबंध करना।
आपदा प्रबंध के मुख्य चरण एवं उद्देश्य।
पहले से तैयारी- इसके अंतर्गत समुदाय को आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैय करने के लिए कार्य करना, जैसे कि
- समुदायिक जागरूकता और शिक्षा।
- समुदाय स्कूल, व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करना।
- प्रशिक्षण अभ्यास।
- आवश्यक सामग्री।
- चेतावनी प्रणाली।
- पारस्परिक सहायता व्यवस्था।
राहत एवं जवाबी कार्यवाही – आपदा से पहले, आपदा के दौरान, और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा के प्रभाव कम से कम हो। इसके अंतर्गत आवश्यक बातें हैं।
- आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना।
- संसाधन जुटाना।
- रहने के लिए अस्थाई व्यवस्था करना।
- बचाव दलों की तैनात करना।
- प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढ कर बचाव करने के लिए दल भेजना।
- आश्रय और टॉयलेट की व्यवस्था करना।
सामान्य जीवन स्तर पर लौटना – ऐसे उपाय जो कि भौतिक आधारभूत सुविधाओं के फिर से निर्माण तथा आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याण की प्राप्त में सहायता हो, जैसे-
- लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देना।
- जिनके परिजन बिछड़ गया उन्हें दिलासा देने के कार्यक्रम।
- अनिवार्य सेवा- सड़कों, संचार संबंधों की पुनः शुरुआत।
- आश्रय आवास सुलभ कराना।
- आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- रोजगार के अवसर ढूंढना।
- नए भवनों का पुनर्निर्माण करना।
रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना – आपदाओं की गंभीरता तथा उनके रोकथाम के उपाय।
- भूमि उपयोग की योजना तैयार करना।
- आपदा घटने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना।
पढ़ा न भूले: पेड़ बचाओ पर निबंध – Save Trees Essay in Hindi
आपदा प्रबंधन संस्थान
भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम 1993 में ब्राजील के रियोड़ीजेनिरो में भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में जापान के याकोहोमा मैं संगठित आदि प्रयास प्रमुख है।
भारत में दैनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ का गठन किया गया। तथा सरकार ने आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी स्थापना की, साथ ही मौसम की सही जानकारी के लिए दूर संबंधी उपग्रहों को भी विकसित किया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित आपदा प्रबंधन संस्थानों को नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपदा प्रबंधन संस्थानों का उद्देश्य, आपदा से ग्रसित क्षेत्र एवं समुदाय की सुरक्षा एवं उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाना है।
डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान आपदा की रोकथाम उनके दुष्प्रभाव को कम करने, और फिर से क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए कार्य करती है, और साथ ही क्षेत्र के लोगों को विशेष सहायता पहुंचाने के लिए अग्रसर होती है।
यह संस्थाएं आपदा से पहले और इसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ समांतर रूप से चलती रहती है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कार्य।
- आपदा प्रबंधन में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- तकनीकी मीडिया की सहायता से आपदा क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों की सूचनाओं से देश को अवगत कराना।
- सभी शिक्षण संस्थाओं जिसे स्कूलों कॉलेजों एवं तकनीकी संस्थानों के लोगों को जागरूक करना।
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समझ कर विकास योजना बनाकर लागू करना।
- किताबों एवं लेख द्वारा बच्चों के पाठ्यक्रम में आपदा से संबंधित विशेष जानकारियों से अवगत कराना।
- राज्य स्तरीय नियमों एवं विकास योजना में आगे बढ़कर योगदान करना एवं संस्थानों को विशेष सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माणों में सहायता प्रदान करना।
Conclusion
दोस्तों हमें उम्मीद है, आपको हमारा “आपदा प्रबंधन पर निबंध”, Disaster Management in Hindi, और Aapda Prabandhan Project File in Hindi से जुडी हर जानकारी का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। हमें आशा है कि आपको Aapda Prabandhan से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो चुकी होंगी। यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एवं कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं।


